बंगाली संस्कृति के विकास में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का योगदान
साभार :गूगल इमेज
बंगाल में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर द्वारा विधवाविवाह प्रारम्भ करने के 10 वर्ष पूर्व बहुबाजार के बाबू नीलकमल बंद्योपाध्याय ने कुछ अन्य प्रबुद्व जनों के साथ मिलकर विधवा पुनर्विवाह कराने की असफल चेष्टा की। 1845 ई0 में बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसायटी ने इस प्रश्न पर धर्मसभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से सम्पर्क साधा, लेकिन दोनों संगठनों ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 1853 ई0 में गुजरात में एक युवा ने दिवालीबाई नामक एक विधवा से विवाह कर इस आन्दोलन को तीव्र कर दिया। नदिया के महाराजा श्रीसचंद्र और वर्द्वमान के महाराजा महातबचंद के अनुकूल रूख की सूचना ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने गवर्नर जनरल के परिषद् के सदस्य जे0 पी0 ग्रांट को दी। इधर महाराष्ट्र में बाबा पद्मसी की दो पुस्तकें विधवा पुनर्विवाह पर छपी कुटुम्ब सुधर्मा एवं यमुना प्रयत्न। इन दोनों पुस्तकों ने युवाओ को विधवा पुनर्विवाह के लिए चल रहे आन्दोलन में शरीक होने के लिए बाध्य कर दिया।
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने जान - बूझकर एक सुनियोजित योजना के अनुरूप विधवा पुनर्विवाह आन्दोलनों के दौरान शास्त्रों के विरुद्व लोकाचार को एवं रीति- रिवाजों के विरुद्व धर्मशास्त्रों को एक-दूसरे के विपरीत विरोधाभाषी रूप में प्रस्तुत किया। इस प्रयास में विधवाओं के प्रति कठोरता को एक खतरनाक बीमारी बताते हुए विधवाविवाह के पक्ष में धर्मग्रंथों में लिखित उद्धरणों को 1854 ई0 में एक लधु पुस्तिका ’ए प्रपोजल एज टू व्हेदर विडो रिमैरिज शुड बी इंट्रोड्यूस्ड और नॉट?’ के रूप में जनता के सामने रखा। आन्दोलन में विद्यासागर ने पराशर स्मृति जैसे धर्मग्रंथों का सहारा लिया। उन्हांने जो विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत किए वह मानवीयता और आंग्ल-हिन्दू कानून के अनुरूप थे। ब्राह्यणीय परम्परा के विधान और औपनिवेशिक कानून एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी परस्पर संगुम्फित थे। कानून राज्य के विधायन का बाहरी मामला था जबकि सुधार धर्मशास्त्रों एवं सामुदायिक विवेचन के माध्यम से होनेवाला एक तरीका था। राजा राधाकांतदेव ने विधवा पुनर्विवाह के विरोध में जो याचिका तैयार की थी जिस पर 36 हजार 764 व्यक्यिं के हस्ताक्षर थे, में भी शास्त्रों एवं परम्परागत रीति- रिवाजां के हवाले से कहा गया था कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम - 1856 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित विधेयक एवं ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिनियमों से काफी भिन्न है। इस याचिका में 1772, 1793 और 1831 में विभिन्न मुकदमों की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों के निर्णय एवं 1837 में स्थापित लॉ कमीशन के समक्ष प्रस्तुत सदर निजामत अदालत के मुख्य न्यायाधीश के विचार शामिल किए गये थे जो हिन्दू कानून के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दिए जाने के सम्बन्ध में थे। इसका जुडवॉँ संस्करण नदिया, त्रिवेणी, भाटपारा, बाँॅसबेरिया, कलकŸा एवं अन्य स्थानों के हिन्दू कानून के अध्येताओं द्वारा तैयार कर विधवा पुनर्विवाह के विरोध में प्रस्तुत किया गया था।11
विधवा पुनर्विवाह आन्दोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए विद्यासागर ने दो पुस्तिकाओं की रचना की। प्रथम, विधवाविवाह एतद्विषयक प्रथम प्रस्ताव एवं दूसरा, विधवाविवाह एतद्विषयक द्वितीय प्रस्ताव। इनका प्रकाशन स्वतंत्र रूप से 1855-56 में कराया गया तथा इन दोनां को मिलाकर 1856 ई0 में एक पुस्तक की शक्ल दी गई जिसका शीर्षक था ‘मैरिज ऑफ हिन्दू विडोज‘। इस क्रम में विद्यासागर ने कलकŸा के दलपतियों का समर्थन हासिल करने का प्रयत्न किया जिसका हिन्दू समाज पर एकाधिकार चला आ रहा था। ये दलपति 19वीं शताब्दी में कलकŸा एवं उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में दलों के आधार पर संगठित थे। उन्होंने राजा राधाकांतदेव के भतीजे के सहयोग से शोभा बाजार के राजा को अपने पक्ष में करने का विफल प्रयास किया। फिर भी उन्हें 1855 में विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में वायसराय को प्रस्तुत की जानेवाली याचिका के निर्माण में हिन्दू समाज के प्रभुत्वशाली वर्गां, जमींदारों, संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षकों, ब्रह्मसमाज एवं यंग बंगाल के समर्थकां तथा तर्कवाचस्पति तारानाथ जैसे पंडितो का सक्रिय सहयोग हासिल हुआ। इस याचिका पर हस्ताक्षर करनेवाले 25 हजार लोगों में टैगोर घराने के दोनो धड़ो का प्रतिनिधित्व करनेवाले देवेन्द्रनाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, वर्द्वमान के महाराजा मेहताबचन्द, नदिया के महाराजा श्रीसचंद्र, उŸारपाड़ा ढाका एवं मैमनसिंह के जमींदार, श्री ताराचंद तर्कवाचस्पति, राजनारायण वसु, दक्षिणा रंजन मुखर्जी, अक्षयकुमार दŸा, जयकृष्ण मुखर्जी, पी0 चरण सरकार और काली कृष्ण मित्रा आदि शामिल थे।
ईश्वरचन्द्ऱ विद्यासागर के विधवा पुनर्विवाह के अभियान को समाचार पत्रों में व्यापक स्थान मिला। प्रशंसा के कुछ गीतां का उल्लेख करते हुए सुमन्त बनर्जी ने टिप्पणी की है कि इनमें से अधिकांश विधवा के आवाज में थे तथा विधवाएॅँ अपने वैधव्य से निकलकर पुनर्विवाह के लिए तैयार थी और उनकी खुशी का इजहार इन गीतां में किया गया। यहाँॅ तक कि शांतिपुर के जुलाहे भी इस अभियान में शामिल हो गए और उन्होंने अपने साँॅचों में तैयार होने वाले कपड़ां पर इन गीतां की पंक्तियॉँ बुन दी।12 इसके पश्चात् विद्यासागर ने अपनी पुस्तिका का अंग्रेजी अनुवाद कर अंग्रेज अधिकारियों को सौप दिया। उनकी सलाह पर ही विद्यासागर ने 1855 ई0 में भारत के गवर्नर जनरल को विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए एक याचिका दी। उसी वर्ष विद्यासागर की याचिका पर आधारित एक कानून का मसौदा विधान परिषद् में जे0 पी0 ग्रांट द्वारा प्रस्तुत की गई।13
इन विरोधाभासी परिस्थितियों में सरकार ने 26 जुलाई 1856 को हिन्दू विधवाओं के लिए हिन्दू विधवा पुनर्विवाह कानून - 1856, 15 वें अधिनियम के रूप में पारित कर वैधानिक समाजसुधार का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। इस कानून के अनुसार ईस्ट इंडिया कम्पनी की सीमाओं एवं स्वामित्व के अंतर्गत नागरिक न्यायालयों में लागू कानूनों के अनुसार हिन्दू विधवाएँॅ कुछ अपवादों को छोड़कर एक बार विवाहित होने के कारण कोई दूसरा वैध विवाह अनुबंध करने में अक्षम है तथा ऐसी विधवाओं की संतानें विधवा द्वारा दूसरा विवाह कर लिए जाने के कारण अपनी पैतृक सम्पति को विरासत में पाने के अयोग्य एवं अक्षम है। ऐसे किसी भी विवाह को इस आधार पर अवैध नहीं माना जाएगा कि स्त्री का पहले ही विवाह हो चुका है या उसकी किसी दूसरे व्यक्ति से सगाई हुई थी और व्यक्ति विवाह के समय मर गया था। विधवा पुनर्विवाह के कारण किसी सम्पिŸा या दूसरे अन्य अधिकारों से वंचित नहीं होगी तथा प्रत्येक विधवा को पुनर्विवाह के पश्चात् विरासत के वहीं अधिकार प्राप्त होंगे जो कि उसके पहले विवाह के समय थे।14
किसी भी हिन्दू अविवाहित कन्या के विवाह को वैध मानने के लिए जो भी शब्दोच्चार किया जाता है या संस्कार सम्पन्न किए जाते है या सगाई की जाती है उसी प्रकार के सभी संस्कार हिन्दू विधवा के विवाह के समय भी सम्पन्न हांगे। किसी भी विवाह को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकेगा कि उपरोक्त संस्कार, शब्दोच्चार या सगाई विधवा के मामले में लागू नहीं होते । यदि पुनर्विवाह करनेवाली विधवा नाबालिग है तथा पहला विवाह पूरी तरह सम्पन्न नहीं हुआ है तो वह अपने माता-पिता, दादा-दादी, बड़े भाई, किसी के न रहने पर अपने किसी नजदीकी पुरुष सम्बन्धी की सहमति के बिना विवाह नहीं कर सकती है। अगर कोई विधवा बालिग है या उसका पहला विवाह पूरी तरह सम्पन्न हो चुका है तो दूसरा विवाह करने के लिए उसी की सहमति को विधिसम्मत् एवं पुनर्विवाह के लिए पर्याप्त माना जाएगा।
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू होने के बाद ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने कई अवसरों पर विधवा पुनर्विवाह समारोहों का आयोजन किया। इस कानून के तहत प्रथम विधवाविवाह पंडित रामधन तर्कवागीश के पुत्र श्रीसचंद्र विद्यारत्न और ब्रह्मानन्द मुखोपाध्याय की 10 वर्षीया विधवा पुत्री कालीमति के बीच सम्पन्न हुआ। तत्पश्चात् कुछ बंगालियों ने उत्साहपूर्वक अपनी विधवा पुत्रियां का विवाह सम्पन्न कराया। ईश्वरचन्द्र मित्रा की बारह वर्षीया विधवा पुत्री का विवाह मधुसूदन घोष के साथ हुआ। मित्रा कोलकता के और घोष पानीहाटी के निवासी थे। इससे पूर्व महाराष्ट्र प्रांत के अहमदाबाद म्यूनिसिपल कार्यालय में लिपिक के तौर पर कार्य करनेवाले एक गौड़ ब्राह्यण रधुनाथ जनार्दन ने छीमाबाई नामक एक विधवा से विवाह किया था।15 हिन्दू पैट्रियाट के अनुसार 1867 में विद्यासागर ने ऐसे 60 विधवा विवाह अपने खर्चे से सम्पन्न कराये। बंगाल के बुद्विजीवियों ने उनके कर्ज को खत्म करने के लिए चंदा देने की पेशकस की जिसे उन्होंने नम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। ढाका डिवीजन में विद्यासागर के निबन्धों ने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में उŸोजना एवं प्रदर्शन को इतना तीव्र कर दिया कि उन्हें बाध्य होकर इनका पुनर्मुद्रण करवाना पड़ा। पूर्वी बंगाल के कई क्षेत्रों विक्रमपुर, बारीसाल, मैमनसिंह, चटगॉँव, और सिलहट में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर अल्पज्ञात व्यक्ति थे परन्तु ब्रह्मसमाजियों की इन इलाकों में पैठ के कारण इस आन्दोलन के प्रति लोगां का उत्साह चरमोत्कर्ष पर पहुँॅच गया था। हजारों गीत एवं कविताएॅँ रच डाली गई, कई हास्य प्रदर्शनों का आयोजन हुआ तथा बुद्विजीवियों ने सभाभवनों में विधवाविवाह के समर्थन में कई छोटी- बड़ी सभाएँॅ आयोजित की। यहॉँ तक कि छोटी समझी जानेवाली जातियों के लोग जैसे कुली, दरवान, किसान, और गाड़ीवान तक भी पूरे रंग में दिखे। शांतिपुर के जुलाहों द्वारा महिलाओं की साड़ी पर उकेरी उन पंक्तियों को काफी प्रसिद्वि मिली जिसमें विद्यासागर के दीर्घजीवी होने की कामना की गई थी। कानून पारित होने की पूर्व संध्या पर जुलाहां ने निम्न पंक्तियॉँ उकेरी थी ‘सुबह की पहली किरण के साथ विधवा पुनर्विवाह कानून लागू होने की सार्वजनिक घोषणा की जाएगी। सभी प्रान्तों, सभी जिलों में विधवा विवाह होने लगेंंगे; हमलोग खुशीपूर्वक अपने जीवन साथी के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। जब अगली सुबह होगी विधवाओं के सारे दुःख दूर हो जाएगें‘। ब्रह्यसमाजी गुरूचरण महालनोविस 1862 ई0 में एक विधवा से विवाह करने के लिए हिन्दू धर्म त्यागकर ब्रह्यसमाजी बन गये जबकि महालनोविस परिवार हिन्दू बना रहा फिर भी दोनां परिवारों के मध्य सदैव मधुर सम्बन्ध कायम रहे।
ब्ांगाल में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की तरह किए गए आन्दोलन की तर्ज पर मुम्बई में विष्णु शास्त्री ने एक आन्दोलन चलाया। उन्होंने 1866 ई0 में विडो मैरेज एसोसियेशन की स्थापना की थी। हिन्दू सम्प्रदाय के कई दलों ने क्रिश्चियन मिशनों के आदर्श पर विधवाश्रमों की स्थापना करने का प्रयत्न किया। पहला विधवाश्रम ब्रह्मसमाजी शशिपद् बनर्जी के द्वारा कलकता के निकट बारानगर में स्थापित किया गया। लेकिन कुछ ही दिनों के पश्चात् सुधार की भावना समाप्त हो गई और आश्रम में ताला लटक गया। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक विधवाओं की दशा के प्रति मायने बदल गये। मालावारी के अभियानों ने विधवाओं के साथ-साथ बाल विधवाओं की समस्याओं पर भी रौशनी डाली थी। बालविवाह की समस्या तो सुधारवादी पुनरुत्थानवादी विवाद में उलझकर रह गयी जबकि विधवाओं की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। शायद इसका कारण यह रहा होगा कि इसके लिए अब तक कानून बनाने के लिए कोई सशक्त आन्दोलन नहीं चलाया गया था। इस समय तक समाजसुधारकों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया था कि कानून बनाने से परिवŸार्न बहुत कम और धीमा होता है। वे स्वर्णकुमारी देवी के इस मत से प्रभावित दिखे कि अब हमें सेवा तथा आत्मसहायता के कदम उठाने चाहिए। विधवाओं की दशा सुधारने के इस चरण में अनेकानेक विधवाएॅँ आकर्षित होकर इससे जूड़ गई जिसके परिमाणस्वरूप सुधार अभियान को नया आयाम मिला।
सावित्रीबाई फुले ने 1852 ई0 में महिला मंडल की स्थापना कर विधवाओं के प्रति सामाजिक विद्वेष के खिलाफ स्त्रियों की मोर्चाबन्दी कर सामाजिक बदलाव के लिए संघर्ष किया। विधवाओं के सिर मुॅँड़ाने जैसी कुरीतियों के खिलाफ फुले ने नाईयों से विधवाओं के बाल न काटने की मार्मिक अपील की। इसके खिलाफ चले अभियान में काफी संख्या में नाईयों ने भाग लिया तथा विधवाओं के बाल न काटने की शपथ ली । विधवाओं के साथ अनैतिक सम्बन्ध बनाने के कारण अवैध बच्चों की उत्पिŸा की शिकार महिलाओं के लिए सावित्रीबाई ने भारत का पहला बालहत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की तथा ऐसी निराश्रित असहाय महिलाओं के लिए एक अनाथाश्रम की स्थापना की।16 29 दिसम्बर 1889 को इंडियन नेशनल सोशल कांफ्रेंस के मंच से रमाबाई ने बाल विधवाओं का सवाल सार्वजनिक मंच से उठाया और मांग की कि विधवा के मुंडन की प्रथा पर रोक लगाई जाए। 1886 में स्वर्णकुमारी देवी ने साखी समिति की नींव डाली। समिति का पहला उद्देश्य अनाथों एवं विधवाओं की सहायता करना था।17 दिल्ली में आज्ञावती नामक जुझारु राष्ट्रवादी कार्यकŸार् जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा अत्यंत सख्त महिला के रूप में सम्बोधित किया गया था, ने स्वर्ण कुमारी देवी के विचारां से एक कदम आगे बढ़कर कहा कि साखी समिति को विधवाओं को पढ़ाने का प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार हो और वे आत्मनिर्भर बन सके। गृहविभाग की सूचना के अनुसार आज्ञावती ने एक विधवाश्रम की स्थापना की थी जिसमें स्त्रियों को राष्ट्रवादी राजनीति का प्रचार करने की शिक्षा दी जाती थी। लीलावती नामक एक ब्राह्यण महिला ने ईश्वरचन्द्र विद्यासागर को 1872 में पारित विशेष विधवा कानून के तहत 1890 के दशक में विधवा पुनर्विवाह कराने में सहायता की थी।18
विधवा सुधार आन्दोलन को गति देनेवालों में डी0 के0 कार्वे प्रमुख सुधारक थे। उन्हें महाराष्ट्र में विधवाओं के पुनर्वास अभियान का जनक माना जाता था। मद्रास से 1901 ई0 से छपनेवाली इंडियन लेडीज मैगजीन के एक लेख में उनके कार्यां की काफी प्रशंसा की गई थी। अपनी विचारधारा को मूर्त रूप देते हुए डी0 के0 कार्वे ने 11 मार्च 1893 को आनन्दीबाई जोशी (गोदूबाई) नामक विधवा से विवाह कर विधवाविवाह सम्बन्धी सामाजिक प्रतिबंध को चुनौती दी। इसके लिए उन्हें घोर कष्ट सहने पड़े। मुरुण्ड में उन्हें समाजवहिस्कृत कर दिया गया तथा उनके परिवार पर भी अनेक प्रतिबंध आयद किए गये। कार्वे ने एक विधवाविवाह संध की स्थापना की किन्तु उन्हें शीध्र ही इस सत्य का अहसास हो गया कि गिने - चूने विधवा पुनर्विवाह सम्पन्न कराने अथवा विधवाविवाह का प्रसार करने मात्र से विधवाओं की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अधिक आवश्यकता इस बात की है कि विधवाआें को शिक्षित कर उन्हें अपने पैरो पर खड़ा किया जाए ताकि वे सम्मानपूर्ण जीवन जी सकें। 1896 ई0 में उन्होंने अनाथ बालिकाश्रम एसोसियेशन बनाया और जून 1900 ई0 में पूणे के पास हिंगले नामक स्थान पर अनाथ बालिकाश्रम की स्थापना की।19
विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारम्भ विधवा पुनर्विवाह के समर्थन से किया। 1865 में उन्होंने विधवा विवाह उŸोजक मंडल की स्थापना की तथा उसके सचिव पद को संभाला। दर्शन को व्यक्तिगत जीवन में लाते हुए उन्होंने 1875 ई0 में एक विधवा से विवाह किया था। महादेव गोविन्द राणाडे महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह का पक्षपोषण करनेवाले काफी सशक्त हस्ताक्षर थे। 1887 ई0 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कांफ्रेंस के मंच से उन्होंने विधवाओं की स्थिति पर प्रकाश डाला था। उन्होंने विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा स्थापित विडो मैरिज एसोसिशन की सदस्यता स्वीकार करते हुए एक ग्यारह वर्षीया विधवा रमाबाई रानाडे से विवाह किया। वी0 एम0 मालावारी ने विधवाओं की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने के लिए इंडियन स्पेक्टेटर्स नामक एक जर्नल का प्रकाशन प्रारम्भ किया। इसके पश्चात् उन्होंने 1884 ई0 में अपने दो नोट - ’नोट ऑन इंफेंट मैरेज इन इंडिया’ और ’नोट ऑन इन्फोर्स्ड विडोहुड’ प्रकाशित करवाया। अहमदाबाद निवासी महिपत्रम ने 1892 ई0 में अहमदाबाद में एक संगठन खड़ा किया जिसका उद्देश्य अहमदाबाद में असहाय रूप से भटकते हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को आश्रय उपलब्ध करना था। इसमें उन्होंने परित्यक्त एवं विधवा महिलाओं को भी शामिल कर लिया जो किसी तरह से अपने आर्थिक बोझ को नहीं उठा सकती थी। इसके अतिरिक्त महिपत्रम ने उन विधवाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जो आत्मनिर्भर होना चाहती थी।
19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में दक्षिण भारत में सुधार आन्दोलनों की शुरुआत हुई लेकिन इसकी गति काफी मंद रही। 1874 ई0 में मद्रास में द हिन्दू विडो रिमैरिज एसोसियेशन का गठन किया गया जो अल्पजीवी रहा। यह एसोसियेशन सिर्फ विधवाआें के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने एवं विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में जनमत तैयार करने में ही लगा रहा। 1880 ई0 में दीवान बहादुर रधुनाथ राव ने इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। 1879 ई0 में वीरेशलिंगम द्वारा राजमुन्द्री विडो - रिमैरिज एसोसियेशन स्थापित होने से मद्रास हिन्दू विडो रिमैरिज एसोसियेशन पुनर्जागृत हुआ तथा इसकी देखरेख में कुछ विधवा विवाह सम्पन्न कराये गये।20
1881 ई0 राजमुन्द्री विधवा एसोसियेशन के अंतर्गत प्रथम विधवाविवाह सम्पन्न हुआ। वीरेशलिंगम एवं अन्य सुधारवादियों ने विरोध, घमकी एवं बलप्रयोग की रणनीति अपनाई। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वयंसेवकां के रूप में संगठित किया ताकि कट्टरपंथियों द्वारा किए जानेवाले बल प्रयोग एवं शारीरिक आघात से सुधारवादियों को बचाया जा सके। स्वंयसेवक गॉँवों में गये विधवाओं एवं दुल्हों की तलाश की तथा उन्हें घसीटकर राजमुन्द्री लाए। 1881 - 84 ई0 के दौरान विधवा पुनर्विवाह के प्रति अति उत्साह दिखाई पड़ा। इस अवधि में 10 से अधिक विधवाविवाह कराये गये। उल्लेखनीय तत्व यह है कि इसमें भाग लेनेवाले सभी उत्साही युवा थे। गोदावरी क्षेत्र काकीनाड़ा के स्थानीय व्यापारी पंडैया रामकृष्णैया ने इस आन्दोलन में काफी धन खर्च किया था। उसने घोषणा की थी कि जो कोई व्यक्ति किसी विधवा से विवाह करेगा उसे एक हजार रूपये की थैली दी जाएगी तथा साथ ही उसे वह अपने यहॉँ नौकरी भी देगा। वीरेशलिंगम ने विधवा विवाह के प्रचार-प्रसार हेतु 1883 ई0 में ’सतीहितबोधिनी’ नामक जर्नल का प्रकाशन शुरु किया था जिसमें सिर्फ स्त्रियों के ही लेख प्रकाशित होते थे।21 इसप्रकार राजमुन्द्री विडो रिमैरिज एसोसियेशन की देख रेख में 10 विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया गया जिसमें अधिकांश ब्राह्यण जाति की विधवाएँॅ थी, दो बनिया जाति की तथा एक अंतर्जातीय विवाह था। इन सभी जोड़ों को एसोसियेशन द्वारा न केवल सुरक्षा प्रदान की गई अपितु इनके जीवन-यापन का प्रबंध भी किया गया। 1919 ई0 में वीरेशलिंगम की मृत्यु तक 30 ऐसे विधवा विवाह सम्पन्न करवाये गये।
मद्रास में 1890 ई0 में के0 एन0 नटराजन ने इंडियन सोशल रिफार्मर नामक अखबार शुरु किया जिसने सारे देश में चल रहे सुधार आन्दोलनों को एक सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । 1892 ई0 में युवा हिन्दुओं ने हिन्दू समाजसुधार एसोसियेशन का गठन किया। ये लोग स्वयं को यंग मद्रास पार्टी के रुप में संबोधित करते थे हालांकि ये लोग इंडियन सोशल रिफार्मर से सम्बद्व थे किन्तु वे उसके अंदर भी एक प्रगतिशील चौकड़ी बना ली थी जो पुराने समाज सुधारकों के विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह, बालविवाह, वधूमूल्य तथा देवदासियों द्वारा वेश्यावृŸा किए जाने से निपटने के उनके तरीकां के आलोचक थे।22
विधवा पुनर्विवाह आन्दोलन को तीव्रता प्रदान करने के लिए 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में एक अनोखा तरीका प्रयोग में लाया गया था वह था विज्ञापन का। इस समय भारत के विभिन्न भागों में विधवा पुनर्विवाह के लिए अखबारों में विज्ञापन प्रसारित करने का रिवाज जोर-शोर से प्रचलित हो चूका था। दिलचस्प बात यह है कि यह विज्ञापन उन विधुरों द्वारा दिया जाता था जो विधवाओं से विवाह करना चाहते थे। परन्तु विधवाओं द्वारा इसप्रकार के विज्ञापन दिए जाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। पात्रता की शŸार् के अनुसार विधवा उसी जाति की होनी चाहिए जिस जाति का पति होता था। वांछनीय योग्यता में विधवा का कुँॅवारी या अक्षतयोनि होना अनिवार्य था। यह तत्कालीन पैतृकवादी, ब्राह्यणवादी हिन्दुत्व तथा व्यक्तिगत साहस के मिश्रण को दर्शाता था तथा उस समय के समाज सुधारकों के मनोवृŸा को भी उजागर करता था। विज्ञापनकŸार्, अधिकांश कॉलेजों के शिक्षित व्यक्ति तथा ऊँची जातियों से सम्बन्धित लोग थे। ‘एक विधवा से विवाह करो मुक्तिदाता कहलाओ‘ सिद्वान्त का परिपालन करनेवाले अधिकांश मद्रास कॉलेज जाने वाले युवा ब्राह्यण थे जिन्होंने ब्राह्यण विधवा से विवाह करने के लिए हिन्दू समाचारपत्र में विज्ञापन छपवाया था। लेकिन यह सर्वविदित तथ्य है कि अनेक दक्षिण भारतीय सुधारकों जिन्होंने विधवा से विवाह किया को, समाज से वहिष्कृत कर दिया गया तथा अनेक ऐसे लोगों को अंतिम संस्कार सम्पन्न कराते समय काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। निश्चित तौर पर उस समय किसी नीची जाति की विधवा से विवाह को बड़ी तल्खी से देखा जाता था।
उन्नीसवीं सदी के सुधारवादियों के लिए बालविवाह ऐसी समस्या थी जिससे वे सम्पूर्ण शताब्दी तक टकराते रहे। इस प्रश्न पर लगभग सभी सुधारकां ने चिंतन किया। अक्षयकुमार दŸा, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, गोपालहरि देशमुख, वी0 एम0 मालावारी, रामकृष्ण परमहंस तथा उनके शिष्य विवेकानन्द; सभी ने अपने-अपने तरीके से इस समस्या का निदान ढूढ़ने का प्रयास किया। बालविवाह को अवरुद्व करने का प्रथम प्रयास औपनिवेशिक सरकार द्वारा 1829 ई0 में किया गया जब कम उम्र की लड़कियों के साथ संभोग को बलात्कार घोषित करते हुए मौत की सजा का प्रावधान किया गया। 1846 ई0 में विधि आयोग ने सिफारिश की थी कि 10 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ यौन-सम्बन्धों का निषेध किया जाना चाहिए। इस सिफारिश को 1860 ई0 में सरकार ने स्वीकार करते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 के तहत व्यवस्था की कि 10 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ यौन सम्बन्ध बनाना आपराधिक आक्रमण माना जाएगा।
1860 ई0 में विवाह के लिए रजामंदी की उम्र 10 वर्ष निर्धारित करनेवाला कानून बनने के बाद उन्नीसवीं सदी के उŸारार्द्व में बहरामजी मालावारी द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने तक बालविवाह के विरोध में कोई सशक्त आन्दोलन खड़ा नहीं किया जा सका। बालविवाह के समर्थकां की दलील थी कि बालविवाह के कारण ही भारत का आध्यात्मिक एवं भौतिक पतन हो रहा है या कि बालविवाह ही भारतीय मूल की कमजोरी के लिए जिम्मेदार है। उनका मानना था कि छोटी उम्र में विवाह होने से राष्ट्र की भौतिक शक्ति का ह्नास होता है। इसके कारण राष्ट्र की प्रगति एवं विकास तो अवरूद्ध होता ही है, यह लोगों के साहस एवं ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। कम उम्र में हुआ विवाह समूची पीढ़ी को निर्बल एवं रुग्ण बना देता है। गोपालहरि देशमुख ने कहा कि जहॉँ तक बालविवाह का प्रश्न है जिसे मैं काफी खतरनाक मानता हूँॅ, यह एक ऐसी प्रथा है जो सम्पूर्ण राष्ट्र को कमजोर बनाती है। कच्ची उम्र में विवाह होने के कारण स्त्रियों के प्रजनन अंग ठीक से विकसित नहीं होते, उनको शिशु जन्म के समय अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कई बार अत्यधिक कष्ट के कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। लघुवय की माताओं के बच्चों के सिर जन्म के समय ही दब जाने के कारण ऐसे बच्चे समय से पूर्व ही मर जाते है या दिमागी रुप से कमजोर होकर शेष जीवन मूर्खां की तरह व्यतीत करते है।
बालविवाह विरोधी आन्दोलन में ब्रह्यसमाजियों ने काफी दिलचस्पी दिखाई। बालविवाह का विरोध करते समय अक्षयकुमार दŸा ने अपनी बात के पक्ष में अतीत का हवाला देने या धार्मिक स्वीकृति की कोई खास परवाह नहीं की। उन्होंने जो तर्क प्रस्तुत किए वे मुख्यतया इस बात पर आधारित थे कि इन बातों का समाज पर क्या असर पड़ रहा है या पडे़गा। धर्मग्रंथों में दी गई व्यवस्थाओं का हवाला देने के बजाय उन्होंने बालविवाह के नुकसान के बारे में चिकित्सा विज्ञान के निष्कर्ष सामने रखे। विवाह एवं परिवार के बारे में उन्हांने बहुत ही आधुनिक विचारों को प्रस्तुत किया। उनके अनुसार विवाह से पूर्व लड़का-लड़की को एक-दूसरे से मिलने-जूलने की इजाजत हो, वैवाहिक जीवन का आधार पति- पत्नी की बराबरी और साझेदारी हो तथा तलाक कानूनी एवं परम्परागत दोनां तरीकों से हो।
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने बालविवाह पर 1850 ई0 में अपना पहला निबन्ध ’बाल विवाहेर दोष‘ लिखा था। इसमें सिर्फ धर्मग्रंथों के उद्वरणों को सिलसिलेवार रखा गया है। इस निबंध में बालविवाह, जाति-बिरादरी द्वारा अल्प आयु में तय विवाह, वैवाहिक उत्पीड़न, शिक्षित महिलाआें के प्रति द्वेष एवं सामाजिक निषेध तथा आत्मसंयमित विधवापन के डरावने और विभत्स रूप पर तल्ख टिप्पणियाँॅ की गई है। बंगाल में प्रचलित विवाह संस्कार को उन्हांने प्रणय विवाह के विपरित माना। उनके अनुसार आदर्श विवाह वहीं हो सकता है जो वयस्क मस्तिष्क एवं शरीर के सम्मिलन पर आधारित हो। बालविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1872 ई0 में नेटिव मैरिज अधिनियम पारित किया गया, यह एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। इसमें बहुविवाह पर प्रतिबंध, विवाहविच्छेद या तलाक को मान्यता और विवाह की उम्र बढ़ाये जाने की बात कही गई थी। यह अधिनियम सिर्फ ब्रह्यसमाजियों पर लागू होता था इसकी न्याय की सीमा में हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई एवं बौद्व नहीं आते थे। इसने विवाह के लिए जाति और धर्म की सीमाओं को सिरे से नकार दिया और विवाह की उम्र 10 से 12 वर्ष कर दी।23 इस अधिनियम के पारित होने के बाद हिन्दू धर्म में प्रचलित बालविवाह और पति की मृत्यु के बाद महिलाओं पर अंकुश लगाये जाने को लेकर भारत भर में बहसों का सिलसिला चल पड़ा। इस बहस में बहरामजी मालावारी के लेख ‘नोट्स ऑन इन्फैट मैरेज एण्ड इन्फोर्स्ड विडोहूड‘ से और तेजी आई जिसमें महिलाओं के सहवास की उम्र बढ़ाने के लिए एक संशोधन विधेयक लाने की वकालत की गई थी।24 1887 ई0 में इस बहस को और हवा मिली जब एक शिक्षित मराठी लड़की रूकमाबाई जो बढ़ई जाति से सम्बन्धित थी, अपने तपेदिकग्रस्त बीमार पति दादाजी के साथ जाने से इंकार कर दिया।25े
बी0 एम0 मालावारी ने बाल विवाह के प्रश्न को आर्थिक विषय बताते हुए इस विषय पर सरकार से जनता को संबोधित करने की अपील की थी। उनके अनुसार बालविवाह के कारण जनसंख्या में निरंतर वृद्वि हो रही है जो आिर्र्थक संवृद्वि दर को कम करते हुए आंतरिक संसाधनों को चट कर रही है। जिससे दरिद्रता को बढ़ावा मिला है। बालविवाह को आर्थिक पतन से जोड़ते हुए एम0 जी0 राणाडे ने इस प्रथा पर अविलम्ब रोक लगाने की याचना की थी। उनका मानना था कि बालविवाह से कमजोर नस्ल एवं प्रजाति के बालक पैदा होते है जिससे लगातार मानव संसाधन का ह्नास हो रहा है। अल्पवय में शादी होने से कम उम्र में ही लड़कियाँॅ माँॅ बन जाती है मॉँ और बच्चे के स्वास्थ्य में गिरावट आती है। युवाओं का ध्यान शिक्षा से हटकर आजीविका में लग जाता है अंततः देश की जनसंख्या के एक बड़े भाग के लिए रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो जाता है, जिससे वे भूखमरी का शिकार हो जाते है। उन्होंने सरकार से अपील की कि भारतीय इस विषय पर भूतकाल में लगे प्रतिबंधों के कारण अपनी सहायता करने में असमर्थ है अतः सरकार को आवश्य हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रजाति सम्बन्धी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए पाथेर प्रभु सुधार समिति के अध्यक्ष डॉ0 कीर्तिकर ने अपने दिए कई व्याख्यानों में कहा कि भारतीय महिलायें सिर्फ इसलिए शिक्षा की एकमात्र उŸाराधिकारिणी है कि वह भारतीय प्रजाति की मॉँ है उन्हें स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यवर्धक भोग्य की जानकारी आवश्य होनी चाहिए ताकि स्वस्थ एवं मजबूत बच्चों के जन्म को बढ़ावा मिल सके।
1890 में घटित फूलमनी की घटना ने विवाह की आयु बढ़ानेवाले समर्थकां के लिए उत्प्रेरक का कार्य किया। 11 वर्षीया बंगाली लड़की फूलमनी के साथ उसके पति हरिमैती ने, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, जबरदस्ती संभोग करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। तत्कालीन कानून के अनुसार फूलमनी 10 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी थी, जो सहवास की उम्र थी, इसलिए हरिमैती बलात्कार का आरोपी नहीं था। यह घटना बी0 एम0 मालावारी की उम्र बढ़ाने के अभियान को विशेष बल प्रदान करती थी कि सहवास की उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष किए जाने की उनकी माँॅग कितनी सार्थक थी। इन सब घटनाओं ने ब्रिटिश सरकार को बाध्य किया कि लड़कियों की उम्र बढ़ाये जाने के लिए एक समिति का गठन करें। इस समिति में प्रभावशाली ब्रिटिश नागरिक और आंग्ल भारतीय व्यक्ति शामिल किये गये जिन्होंने महिलाओं के साथ सहवास की उम्र बढ़ाये जाने की सिफारिश की थी।
बी0 एम0 मालावारी ने 1891 ई0 में भारतीय अपराध प्रक्रिया कानून संशोधन अधिनियम - 10 के लिए अभियान चलाया जिसके अनुसार भारतीय दण्ड प्रक्रिया 1860 की धारा 375 एवं हिन्दू विवाह कानून 1882 में संशोधन किया जाना था, जिससे विवाहित एवं अविवाहित लड़कियों के साथ सहवास की उम्र सीमा 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी जानी थी। 1860 के दण्ड प्रक्रिया में विधान था कि कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ 10 वर्ष की उम्र के बाद ही शारीरिक सम्बन्ध बना सकता था। इससे पूर्व किया गया सहवास बलात्कार की श्रेणी में अपराध माना जायेगा और वह व्यक्ति दण्ड का भागी होगा। एज ऑफ कंसेन्ट बिल को 9 जनवरी 1891 ई0 को भारतीय गवर्नर जनरल की तरफ से आन्द्रे स्कोवेल ने कलकता में विधायिका सभा में प्रस्तुत किया था तथा इसी दिन इस बिल पर बहस भी शुरु हो गई। रमेशचन्द्र मित्र ने इस बहस में भाग लेते हुए हिन्दू परम्परा में हस्तक्षेप के आधार पर इसका कड़ा विरोध किया जबकि विधायिका सभा के एक अन्य सदस्य बम्बई के बहादुर कृष्णजी लक्ष्मण नलकर और महिला सामाजिक संस्थान के अध्यक्ष का सर्मथन इस बिल को प्राप्त हुआ। इन बहस में तिलक और अन्य हिन्दू कट्टरपंथियों ने इसका विरोध किया।26
महाराष्ट्र और बंगाल के बुद्विजीवियों ने इस बिल का तगड़ा विरोध किया। हिन्दू कट्टरपंथी और परम्परावादियों के अनुसार यह अधिनियम शक्तिशाली हिन्दू जनता को उद्वेलित करनेवाली थी। महाराष्ट्र में इस अधिनियम के विरोधियों का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे जिन्हें पूना र्सावजनिक सभा के माध्यम से पुनरुत्थानवादियों का भरपूर सहयोग मिल रहा था।27 ये लोग हिन्दू ब्राह्यण और महाराष्ट्र के गौरव की बात कर रहे थे तथा जनता को इसके विरुद्व प्रदर्शन के लिए उकसा रहे थे। तिलक अधिनियम का विरोध इस आधार पर कर रहे थे कि यह हिन्दुओं का आंतरिक मामला है, अंग्रेजों का मामला नहीं है इसे हिन्दुओं को ही सुलझाना चाहिए। ’उन्हें हमारे धर्म, परम्परा एवं रीति-रिवाजों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।’ इस अधिनियम का बंगाल में भी काफी विरोध हुआ तथा इसने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को विस्तार देने में महत्वर्पूण भूमिका निभाई।28
एज ऑफ कंसेंट बिल को महाराष्ट्र की नारीवादियों का अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ। 1890 ई0 में बम्बई की महिलाओं द्वारा प्रथम मेमोरियल समारोह आयोजित किया गया जिसमें ब्रिटिश नारीवादियों की भी प्रमुख भागीदारी रही थी। इस समय इस बिल के समर्थन में महिलाओं की एक समिति कार्य कर रही थी जिसमें ब्रिटेन एवं महाराष्ट्र की प्रभावशाली महिलायें शामिल थी। ब्रिटिश सदस्यों में लेडी रे, डॉ0 पेचे फिप्सन तथा भारतीय सदस्यों में डॉ0 रुकमाबाई, पंडिता रमाबाई, रमाबाई रानाडे और रुकमाबाई मोदक प्रमुख थी। लंदन की नारीवादी संगठन ’मिलिसैंट फाउसेट इंडियन नेशनल एसोसियेशन’ लगातार सरकार पर दबाव बनाये हुए थी कि वह बिल को पारित कराने के पक्ष में निर्णय ले।
भारतीय महिलाओं के हस्ताक्षरयुक्त प्रथम स्मारपत्र 30 दिसम्बर 1890 को प्रस्तुत किया गया। लेकिन प्रथम स्मारपत्र का उŸार नहीं मिलने पर रुकमाबाई मंडोक एवं धावलीबाई सुकथांकेर जैसी महिलाओं के मन में विचार आया कि इसमें सहवास की उम्र 14 वर्ष रखने के कारण ही शायद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा विचार नहीं किया गया है। अतः जब दूसरा स्मारपत्र भेजा गया तो उसमें सहवास की न्यूनतम आयु घटाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। इसी प्रकार का एक स्मारपत्र आर्य महिला समिति की ओर से भी भेजा गया जिसपर 88 महिलाओं के हस्ताक्षर थे जिसमें 65 हिन्दू थी। पूणे के पारसी एवं एंग्लो इंडियन महिलाओं ने इस विषय पर एक अलग याचिका ब्रिटिश सरकार को सांपी थी। 23 फरवरी 1891 ई0 को 128 पारसी एवं 83 देशी ईसाई महिलाओं के हस्ताक्षरयुक्त एक चायिका गवर्नर जनरल को सुपूर्द की गई। इन सभी याचिकाओं की विषयवस्तु अलग - अलग थी। जहॉँ प्रथम स्मारपत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की असंगतता एवं खामियों को उजागर किया गया था वहीं दूसरी याचिकाओं में उन समस्याओं को उठाया गया था, जो स्त्री जाति से सम्बन्धित थे। आर्य महिला समाज द्वारा प्रस्तुत दूसरी याचिका में 514 याचिकाकŸार्ओं ने बिल के विरोधी पुरुष सुधारकों से अपील की थी कि वे इस बिल का विरोध करना छोड़ दे तथा इसके पारित किए जाने में सहयोग करे। यह याचिका आर्य महिला समाज की सचिव घावलीबाई सुकथांकेर ने के0 एल0 नलकर को प्रदान किया था जिसका शीर्षक था ‘514 नैटीव का स्मारपत्र‘। इसप्रकार महिलाओं ने इस बिल के पक्ष में जिस प्रकार के तर्क, प्रदर्शन एवं सभाओं का आयोजन किया था उससे साफतौर पर साबित हो गया था कि यह एक राष्ट्रवादी या धार्मिक मुद्दा न होकर एक लैंगिक मुद्दा बन चुका है। एज ऑफ कंसेंट बिल पर द्वितीय वाचन मार्च 1891 ई0 में शुरु हुआ तथा 19 मार्च 1891 के दिन गवर्नर जनरल लांसडाउन के इस पर हस्ताक्षर होने के साथ ही ब्रिटिश भारत में लागू कर दिया गया। इस कानून को एज ऑफ कंसेंट कानून अधिनियम -10, 1891 के नाम से जाना जाता है। एक्ट के अनुसार लड़कियों के साथ सहवास की उम्र बढ़ाकर 10 वर्ष से 12 वर्ष कर दिया गया था। यह सभी अविवाहित एवं विवाहित लड़कियों पर लागू होनेवाला कानून था इस उम्र से कम आयु की लड़कियों के साथ लैंगिक व्यवहार को बलात्कार की श्रेणी में मानते हुए दंड का विधान किया गया था। यह कानून भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय अपराध प्रक्रिया की धारा-375 और हिन्दू विवाह कानून 1882 में संशोधन कर बनाया गया था।
19वीं शताब्दी के ब्रिटिश भारत के सामाजिक विधायन के इतिहास में 1891 का एज ऑफ कंसेंट बिल एक मील का पत्थर है। यह लम्बे समय से चले आ रहे बहस का चरमोत्कर्ष था, जो वैवाहिक अधिकार के पुनर्स्थापन, तलाक और बालविवाह के मुद्दों पर विचार का केन्द्र बना हुआ था। इसमें सहवास की उम्र बढ़ाकर 10 से 12 वर्ष करने और इसे उल्लंघन को बलात्कार की संज्ञा देते हुए 10 वर्ष के कारावास या आजीवन देश निकाला जैसे दंड का प्रावधान इस बात का सूचक था कि बालविवाह के प्रति कडे़ कदम उठाए जा सकते है। प्रसिद्व समाजसुधारक एवं इतिहासविद् एस0 नटराजन के अनुसार यह कानून भारत में सुधार का अंतिम मापदंड था जिसने ब्रिटिश जनता की विचारधारा को काफी प्रभावित किया। यह सुधार का प्रथम कदम था जब भारतीयों ने वैचारिक तौर पर आवाज बुलन्द की, यह प्रथम अवसर था जब भारतीय नेताओं ने जनसमूह के नेतृत्व करने की क्षमता प्रदर्शित की तथा यह पहला ही अवसर था जब राजनीति और उसकी प्रतिक्रिया सफलतापूर्वक एक-दूसरे से जूड़े हुए थे।29
19वीं शताब्दी के मध्य में बहुविवाह की प्रथा को समाप्त करने के लिए एसोसियेशन ऑफ फ्रेंड्स ने लेजिस्लेटिव कांसिल के सामने एक याचिका दायर की जिसमें मनुस्मृति के नौवे अध्याय के कुछ पद्य उद्घृत करते हुए स्पष्ट किया गया था कि पति किन-किन परिस्थितियों में दूसरी पत्नी रख सकता था। उन्होंने यह विचार सामने रखा कि कुलीन ब्राह्यण धर्मशस्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके एक से ज्यादा पत्नी रख रहे है, पर उन्हें कानूनी वैधता प्रदान नहीं की जानी चाहिए। इसी याचिका में आगे उन्होंने प्रार्थना की कि ऐसी शादियों से जो बच्चे पैदा हो, उन्हें अवैध माना जाए और सम्पिŸा के बॅँटवारे में उन्हें कोई हक न हो। विधवा पुनर्विवाह कानून पारित होने के बाद ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने कुलीनों में प्रचलित बहुपत्नीवाद के खिलाफ अभियान चलाया। उनके इस अभियान में बडे़ पैमाने पर भूमिपति एवं जमींदार शामिल हुए। समाज के उच्चवर्गीय लोगां में यह प्रथा प्रचलन में थी जबकि निम्न आर्य वर्ग के लोग धीरे-धीरे इसे भूल चूके थे। 1856 ई0 से पूर्व इस विषय पर बने कानून 1857 के विद्रोह के दौरान पृष्ठभूमि में चले गये थे। लेकिन विद्यासागर ने 1860 ई0 के बाद इस प्रश्न को पुनः उठाया तथा कुलीनवाद एवं बहुपत्नी प्रथा पर दो निबन्ध प्रकाशित करवाये। इस प्रश्न पर उन्हें हिन्दू कट्टरपंथियों का बचाव करनेवाली प्रमुख संस्था सनातन धर्मरक्षिणी सभा का भी समर्थन हासिल हुआ था।
ब्रह्मसमाजी केशवचन्द्र सेन ने महिला अधिकरिता के दावे को मजबूती प्रदान करने के लिए महिलाओं को समर्पित एक पत्रिका ‘वामाबोधिनी‘ की शुरुआत 1863 ई0 में की थी। 1865 ई0 में महिलाओं के लिए एक अलग संगठन ‘बह्यमिका‘ समाज की स्थापना की। इस समाज ने बहुविवाह का तीव्र विरोध किया। उन्होंने 1859 ई0 में विधवा पुनर्विवाह पर एक नाटक का मंचन किया था जिसमें सेन ने भद्रलोक में प्रचलित कुलीन प्रथा पर गहरी चोट की थी। 1860 ई0 में केशवचन्द्र सेन ने संगत सभा की स्थापना की जिसके सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि वे सार्वजनिक तौर पर होनेवाले महिलाओं के नृत्य-गान में शामिल नहीं होंगे और शराब का सेवन नहीं करेंगे। बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए बंगाल सरकार ने 1867 ई0 में एक समिति गठित की थी। इस समिति में बंगाली और अंग्रेज दोनों शामिल किए गये थे। बंगाली सदस्यों में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, सŸाशरा घोषाल, रामनाथ टैगोर, जयकिशन मुखर्जी एवं दिगम्बर मिŸार शामिल थे। ब्रह्यसमाजी केशवचन्द्र सेन के प्रयासों से 1872 में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए नेटिव मैरिज अधिनियम पारित किया गया जिसे ब्रह्यविवाह कानून भी कहा जाता था। इसमें बहुविवाह पर प्रतिबंध के साथ - साथ विवाहविच्छेद एवं तलाक को मान्यता तथा विवाह की उम्र बढ़ाये जाने के लिए कानून बनाये गये।31
हिन्दुओं में प्रचलित क्रूरतम बुराई बालिका हत्या को रोकने का प्रयास औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा प्रतिबंध आयाद करनेवाली घोषणाओं के रूप हुआ था। सर्वप्रथम 1804 ई0 में बरेली की सरकार ने अपने क्षेत्र में बालिका हत्या पर रोक लगाने हेतु इसके खिलाफ दण्ड की घोषणा की थी। ऐसी ही एक घोषणा 30 जुलाई 1809 ई0 को प्रसारित की गई। 1836 ई0 में आजमगढ़ के मजिस्ट्रेट थाम्पसन एवं 1839 ई0 में इलाहाबाद के मजिस्ट्रेट मांटगु अन्य सभा अपने जिले में आयोजित की। इस सभा में पहाड़ी के रहनेवाले राजपूतां को आमंत्रित किया गया था। इसमें विवाह में होनेवाले अपव्यय पर विचार हुआ और राजपूतों ने भी शिशुहत्या त्यागने और विवाह में अधिक खर्च न करने की प्रतिज्ञा की। गवर्नर जनरल के आदेशानुसार अमृतसर में इस विषय पर एक वृहद् सभा का आयोजन हुआ जिसमें महाराजा, राजा, व्यापारी, कृषक, सिक्ख, हिन्दू मुसलमान सभी एकत्रित हुए थे। इस सभा में तीन दिनों के विचार-विमर्श के बाद सभी ने एक स्वर से शिशु - हत्या की प्रथा का नाश करने की शपथ ली। स्वतंत्र राजाओं ने भी इस बात का वचन दिया कि वह अपनी रियासत में इस प्रथा को समाप्त कर देंगे।
गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में 1808 ई0 में ही कर्नल वाकर द्वारा कन्या शिशुहत्या रोकने की चेष्टा की गई। उन्होंने राव कच्छ के दरबार में फतेह मुहम्मद के माध्यम से एक पत्र भेजकर शिशुहत्या रोकने की अपील की थी। इसके बाद एलफिंस्टन एवं लार्ड क्लेटर ने शिशुहत्या करनेवालां पर जुर्माना लगाया तथा सार्वजनिक सभाओं में उन्हें जलील करने का तरीका अपनाया। 1831 ई0 में कर्नल विलोवी ने इस प्रथा को समाप्त करने हेतु बम्बई गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट भेजी जिसके आधार पर घोषणा की गई कि जो कोई अपनी लड़की को मारेगा उसको सख्त दंड दिया जाएगा और जो कोई व्यक्ति अपनी लड़की को जिन्दा रखेगा उन्हें सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। यह सरकारी घोषणा केवल मृतपत्र बनकर ही नहीं रह गया अपित इसे कार्यरुप में भी परिणत किया गया। राजकोट के ठाकुर सुराजी इस घोषणा के पहले शिकार बने। इनके यहॉँ लड़की पैदा हुई जिसको उन्होंने मार डाला। फलतः उन्हें 12 हजार रूपये जुर्माने के रुप में देने पडे़।
देवदासी प्रथा उन्मूलन अभियान 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरु हुआ जिसमें सुधारवादी दासप्रथोन्मूलनवादी तथा पुनरूत्थानवादी शामिल थे। इस अभियान की वास्तविक शुरुआत 1882 ई0 में हुई थी। 1892 ई0 में गवर्नर जनरल से अपील की गई थी कि दक्षिण भारत एवं उडी़सा में इस प्रथा के उन्मूलन के प्रयास किए जाए। देवदासी प्रथा के उन्मूलन के प्रयास और पुनरुत्थान के दौरान कुछ पत्र-पत्रिकाओं यथा द इंडियन सोशल रिफार्मर एवं लाहौर प्यूरिटी सर्वेन्ट ने सुधारवादियों का साथ दिया। राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, महादेव गोविन्द राणाडे, डी0 के0 कार्वे एवं ई0 वी0 रामास्वामी पेरियार ने इस प्रथा के विरोध में अपनी आवाजें बुलाई की तथा इस प्रथा को एक बुराई के रुप में स्वीकारते हुए इसे समाप्त किए जाने की बात कही। इस मुहिम को सबसे बड़ा समर्थन थियोसोफिकल सोसायटी ऑफ इंडिया की तरफ से हासिल हुआ। इन्होंने अपनी एक शाखा आडियार (चेन्नई) में खोलकर देवदासी प्रथा के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ दिया। इसी समय देवदासी नृत्य की एक विशिष्ट शैली सादिर को भारत के प्राचीन सांस्कृतिक वैभव से जोड़ने की कोशिशें की गई। रूक्मिणी देवी अरुण्डेल ने इस अभियान को काफी तीव्रता प्रदान की। देवदासी नृत्य को नाट्ययोग के रूप में निरुपित किया गया जिससे देवदासियों का आत्मिक उत्थान हो सके। पुनरुत्थानवादी सदिर शैली को संरक्षित करना चाहते थे जिसका कड़ा विरोध देवदासी प्रथा की प्रतिनिधि बाला सरस्वती और अन्य देवदासियों ने किया। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि तत्कालीन परिवेश में सुधारवादियों एवं पुनरुत्थानवादियों में ब्राह्मणों का बाहुल्य था। दासप्रथोन्मूलनवादियों की सख्त राय थी कि कथित अनैतिक यौनकर्म लिप्तता की वजह से इस प्रथा की समूल समाप्ति होनी चाहिए।32
रूक्मिणी देवी अरुण्डेल ने सादिर नृत्यशैली का रूपान्तर भरतनाट्यम में किया जिसे अनपेक्षित रुप से काफी प्रसिद्वि मिली। ब्रिटिश अधिकारी, गैर-ब्राह्यण नेता, ईसाई धर्मसुधारवादी देवदासियों के नृत्य पर प्रतिबंध लगाए जाने के पक्ष में थे। इस संदर्भ में 1893 ई0 में मैसूर सरकार ने एक कानून बनाकर देवदासियों द्वारा अनिवार्य रूप से मंदिरों में किए जानेवाले नृत्य पर पाबंदी लगा दी जबकि इस नृत्य को पूर्णतः प्रतिबंधित करनेवाला कानून 1909 ई0 में ही जाकर पारित हो सका। यह देवदासियों के पुनरुत्थान के लिए बननेवाला पहला कानून था। समाजसुधारकों ने मंदिर नृत्य पर मोर्चा खोलते हुए दो टूक आरोप लगाया कि समाज के अति प्रतिष्ठित लोग ही देवदासी प्रथा का दुरुपयोग वेश्यावृŸा या व्यवसाय के रुप में करते है। 1911 ई0 में रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में देवदासी प्रथा के विरुद्व देशव्यापी जनान्दोलन चलाये जाने का फैसला किया गया। विट्ठल रामजी शिन्दे ने इस प्रथा को अमानवीय करार देकर इसके खिलाफ पुरजोर प्रयास किया। उनके सहयोग से पश्चिम हिन्दुस्तान की कन्याओं के रक्षार्थ एक संस्था सर्वधर्मी की स्थापना हुई। इस संस्था के अध्यक्ष मुम्बई के विशप तथा तीन उपाध्यक्ष क्रमशः नारायण चन्द्रावरकर, जी0 के0 पारिख और भालचन्द्र कृष्ण थे। विट्ठल रामजी शिन्दे ने सचिव पद संभाला। उनका विचार था कि समाज के सभी लोग एकजुट होकर आन्दोलन करे तो देवदासी प्रथा का विनाश किया जा सकता है। राजसता या धर्मसŸा इस कुरीति के उन्मूलन में सक्षम नहीं है। डॉ0 एम0 जी0 भंडारकर ने मुरलीप्रथा के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। इस प्रथा के अंतर्गत जेजुरी जैसे स्थान पर मुरुकिया अपने कब्जे में रहनेवाली कन्याओं का विवाह देवी से उस समय कर देती थी जब वे कन्याएॅँ अबोध होती थी। बाद में उन्हें वेश्यालय में भेज दिया जाता था। भंडारकर ने एक प्रस्ताव के जरिए सरकार से मांग की कि वह सख्त कानून बनाकर ऐसी महिलाओं को सजा दिलाए।
वेश्याओं की स्थिति में सुधार की पहली कोशिश कलकता के माइकेल मधुसूदन दŸा द्वारा की गई। उन्होंने वेश्याओं को थिएटर का कलाकार बनने का प्रस्ताव किया था। अपने प्रस्ताव की मंजूरी के लिए दŸा ने उसे बंगाल थियेटर कमेटी के पास भेजा। इसके बाद व्यावसायिक थियेटर में स्त्रियों की भूमिका अदा करनेवाले पुरुषों का स्थान वेश्याओं ने ले लिया। अनेक वेश्याएँॅ नायिकाएँॅ बन गई जिनमें से विनोदिनी बहुत बड़ी अदाकारा के रूप में उभरी। प्रगतिशील समझ रखने वाले विद्यासागर ने स्वयं मधुसूदन दŸा के प्रस्ताव का विरोध किया। बंगाल थिएटर समिति ने जब मधुसूदन दŸा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो विद्यासागर ने बंगाल थिएटर समिति से त्यागपत्र दे दिया। अनेक सुधारक इससे व्यथित हुए कि अनेक वेश्याएँॅ उनकी अपनी या समान जातियों की तथा आर्थिक समुदायों से आई थी। दŸा वेश्याओं के पुनर्वास के लिए सकारात्मक प्रयास करते नजर आए। जबकि अधिकांश सुधारक उनकी दशा सुधारने के प्रयास के बजाए वेश्याओं के प्रति अपनी धृणा दर्शाने के लिए चिन्तित दिखाई पड़े। नाच-गान पर प्रतिबंध लगाने का अभियान पहली बार मिशनरी प्रभाववाले संगठन लीग फॉर सोशल प्यूरिटी एण्ड टेम्परेंस द्वारा चलाया गया जिसने सरकार के समक्ष याचिका प्रस्तुत की कि सार्वजनिक समारोहों में सरकार द्वारा प्रायोजित सभी प्रकार के नृत्यगान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए। शताब्दी के अंत तक सुधारकों के साथ-साथ नाच विरोधी अभियान इतना लोकप्रिय हो गया कि 1897 में न्यायमूर्ति रानाडे ने घोषणा की कि आज के बाद सभी समाजसुधार संगठन कृतसंकल्प हे कि वे अपने परिवारों में होनेवाले विवाह या अन्य समारोहों में नाच की अनुमति नहीं देंगे और नहीं उन समारोहों में शरीक होंगे जहाँॅ नाच की व्यवस्था होगी।33
कांग्रेस अधिवेशनों के माध्यम से महिलाओं ने जिन समस्याओं को उठाया उनमें वेश्यावृŸा पहला एवं प्रमुख मुद्दा था। 1888 ई0 के कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके कहा गया था कि वेश्यावृŸा सम्बन्धी कानून के उन्मूलन के प्रयास में उनका समर्थन करनेवाले भारतीय ब्रिटिश शुभचिंतकों के साथ सहयोग करने को भी तैयार है ताकि भारत में सरकार द्वारा निर्धारित वेश्यावृŸा का नियमन करनेवाले नियम कानूनों को समाप्त कराया जा सके। वेश्यावृŸा सम्बन्धी ब्रिटिश कानून का संगठित विरोध 1864 ई0 में शुरु हो गया था। इस वर्ष सरकार ने संक्रामक रोग अधिनियम पारित कर वेश्याओं के चिकित्सकीय जाँॅच एवं पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया। अखबारों में खबरें प्रकाशित हुई कि अनेक वेश्याओं ने पुलिस उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। बंगाल प्रेसीडेंसी में जेलों के ऊपर जारी एक प्रशासनिक रिपोर्ट में कहा गया कि कानून का उल्लंधन करने के जूर्म में औसतन एक दर्जन वेश्याएँॅ रोजाना गिरफ्तार की गई।34 ब्रिटेन में भी इस कानून के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ तथा ईसाईयों ने सघन विरोध अभियान चलाते हुए इस कानून की आलोचना की। उन लोगों का कहना था कि सरकार ने वेश्यावृŸा को समाप्त करने के बजाय उसे कानूनी जामा पहना दिया है; भारत में यह तर्क 1870 के बाद के दशक में दिया जाने लगा था।
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जैसे राष्ट्रवादियों ने वेश्यावृŸा पर नागरिक स्वतंत्रता की तर्ज पर तर्क प्रस्तुत किए। 1895 में सरकार की ओर से पुलिस को और अधिक शक्ति प्रदान की गई। ताकि कोई भी भारतीय सिपाही बिना किसी साक्ष्य के भी किसी भी औरत को वेश्यावृŸा के आरोप में गिरफ्तार कर सके। इस आशय का एक बिल प्रस्तुत किए जाने पर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने तीव्र विरोध करते हुए कहा कि इससे पुलिस की निरंकुशता बढ़ जाएगी साथ ही इससे व्यक्तिगत आजादी को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। उनके विरेध के परिणामस्वरुप बिल में संशोधन किया गया तथा पुलिस अधिकारियों को केवल उसी स्त्री को वेश्यावृŸा के आरोप में गिरफ्तार करने की अनुमति दी गई जिसके विरुद्व लिखित एवं स्वतंत्ऱ शिकायतें की गई हो।
19वीं शताब्दी में अंग्रेजों को अभिव्यक्ति का तरीका जो बेहद नापसंद था तथा तत्कालीन समाज सुधारकों का ध्यान भी अपनी तरफ आकृष्ट कर रहा था वह था पेशेवर महिलाओं द्वारा सार्वजनिक शोक प्रदर्शन। राष्ट्रीय सामाजिक कांफ्र्रेंस के नौवें अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर पंजाब में स्त्रियों द्वारा किसी की मृत्यु पर छाती पीट - पीटकर तथा चिल्लाकर शोक- प्रदर्शन करने की प्रथा ‘स्यापा‘ को आपिŸाजनक तथा अनुचित करार देते हुए इसकी तीव्र भर्त्सना की गई थी। सम्मेलन में सभी समाजसुधार संगठनों से स्यापा के विरुद्व अभियान चलाने का आहवान किया।
उन्नीसवीं शताब्दी के लगभग सभी सुधारकों ने माना कि पर्दाप्रथा के कारण ही महिलाओं में अशिक्षा की स्थिति बनी हुई है। फिर भी पर्दाप्रथा के खिलाफ कोई सशक्त अभियान नहीं चलाया जा सका। लोगां में शिक्षा एवं उदारवादी तथा बुद्धिवादी विचारों के प्रसरण से पर्दाप्रथा समाप्त होने लगी। भोपाल की बेगमों, आर्यसमाज, ब्रह्मसमाज तथा अन्य संगठनों ने इसके लिए आन्दोलन खड़े किये। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि परदा का सामाजिक प्रगति के साथ - साथ मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक जीवन के उत्थान में अगर औरतों को अपनी भूमिका अदा करनी है, अगर उनके लिए जानना जरुरी है कि किन कŸार्व्यों एवं उŸारदायित्वों के लिए उनके लड़कों को प्रशिक्षित किया जाना है तो परदा को खत्म होना ही चाहिये।35 1865 ई0 में ब्रह्मसमाज की शाखा ब्रह्ममिका समाज ने पर्दाप्रथा हटाने एवं अंतर्जातीय विवाह अयोजित किए जाने के प्रति काफी उत्साह दिखाया। स्वर्ण कुमारी देवी ने 1884 ई0 में पर्दाप्रथा को समाप्त किए जाने के लिए एक लेख वामाबोधिनी पत्रिका में लिखा जिसमें पर्दा को हटाए जाने की वकालत की थी।
उन्नीसवीं सदी में जब सती प्रश्न प्रगति और आधुनिकता विषयक संवादों का अंग बन गया तो उपनिवेशित पुरुषों की नई सती के लिए तलाश के अंग के रूप में स्त्री-शिक्षा का एक आन्दोलन शुरु हुआ। गेराल्डाइन फोर्बेस के अनुसार तीन समूह शिक्षा-प्रसार के निमित बने अंग्रेज शासक, ईसाई मिशनरियाँ, पुरुष सुधारक एवं शिक्षित भारतीय स्त्रियॉँ। सर्वप्रथम, ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में बालिका विद्यालयों की स्थापना की गई, परन्तु उन्हें भारतीय समाजसुधारकों से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। 19वीं शताब्दी के मध्य तक सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के बुद्विजीवी समाजसुधारकों के सहयोग से भाषायी आधार पर बालिका विद्यालय खोले जाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंत तक मध्यवर्गीय शिक्षित महिलाओं द्वारा कई शिक्षण संस्थान स्थापित किए जा चूके थे तथा उनके बीच बहस के केन्द्र में स्थापित प्रश्न था कि कौन सा शैक्षिण मॉडल महिलाओं के लिए अत्यधिक अनुकूल होगा। 19वीं शताब्दी के उŸारार्द्व तक कुछ ही महिलायें शिक्षा के लिए चल रहे अभियानों का हिस्सा बन पाई थी। लेकिन दौर बदला, माहौल बदला, 20वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षां में ही महिलायें शिक्षा के लिए विषय चयन के साथ-साथ पाठ्य-योजना तैयार कर कन्या पाठशालाएॅँ स्थापित करने लगी थी।
19वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में तुलनात्मक रूप में लड़कों के विद्यालयों को सरकारी अनुदान मिलता रहा जबकि कन्या शिक्षा के प्रति ब्रिटिश अधिकारी लगभग उदासीन ही रहे। उदारवादियां एवं ईसाई मिशनरियों के काफी दबाव के बावजूद भी सरकार ने महिला शिक्षा के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। स्त्री शिक्षा का क्षेत्र ईसाई मिशनरियों के लिए रूचि का विषय बना; क्योंकि धर्मान्तरण एवं धर्मप्रचार के लिए महिलाएँॅ आसान लक्ष्य साबित हो सकती थी। सर्वप्रथम, 1789 ई0 श्रीमती कैम्पवेल और डॉ0 एण्ड्रुवेल ने मद्रास में एक महिला बालिकाश्रम की स्थापना की थी। मिशनरियों द्वारा पहला बालिका विद्यालय मे ;डंलद्ध के निर्देशन में बंगाल के चिन्सुरा में स्थापित किया गया।
1816 ई0 में घड़ीसाज डेविड हेयर द्वारा हिन्दू कॉलेज की स्थापना के बाद 1818 ई0 में कलकता विद्यालय समिति की स्थापना की गई जिसका प्रमुख उद्देश्य कन्याओं को बालकों के समान ही शिक्षा दिए जाने का प्रबंध करना था। राजा राधाकांत देव इस संस्था के प्रथम एवं एकमात्र सचिव थे, जो आगे चलकर महिला शिक्षा के संरक्षक भी बने। राधकांत देव ने महिला शिक्षा पर 20 से अधिक निबन्ध लिखे। परम्परावादी धडे़ की अगुयाई करने के बावजूद भी उनकी इच्छा थी कि लड़के एवं लड़कियॉँ एक साथ विद्यालय में प्रवेश पाए; जबकि उनके इस सहवŸार् शिक्षा के विचार को हिन्दू समाज के उदारवादी समझे जानेवाले सुधारवादियों का भी समर्थन हासिल नहीं हो सका। स्त्री शिक्षा से सम्बन्धित पहली पुस्तक किसी भारतीय भाषा में 1819 ई0 में गुरुमोहन सेन द्वारा बांग्ला में लिखी गई जिसे 1820 ई0 में राधाकांत देव के प्रयासों से कलकता की कन्या बाल समिति द्वारा प्रकाशित किया गया था।
उन्नीसवीं सदी के मध्य तक बंगाल खासतौर पर कलकता में स्त्रियों की शिक्षा का मुद्दा उदार हिन्दुओं, ब्राह्यणों और प्रगतिशील छात्रों के लिए आन्दोलन का विषय बन चुका था। मिशनरी विद्यालयों द्वारा ईसाईयत फैलाने के डर से हिन्दू और ब्राह्यण पाठशालायें खोली जा रही थी। 1819 ई0 में कलकता फीमेल जुबेनाइल सोसायटी ने जिसका गठन राधाकांत देव के सहयोग एवं परामर्श से बापटिस्ट सोसायटी ने किया था, उŸारी कलकता के गौरी बाजार में कन्याओं के लिए एक स्कूल स्थापित किया। लंदन मिशनरी सोसायटी के तहत कार्य करते हुए श्रीमती गोगरली ने 1820 ई0 में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जिसमें इंगलिश के साथ - साथ बंगाली भाषा में पढ़ने-लिखने की सुविधा थी। इस विद्यालय में सिलाई, बुनाई, भूगोल और बाइबिल का ज्ञान कराया जाता था। जून 1824 ई0 में क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी की संचालन समिति ने नारी शिक्षा के विकास के लिए अपना उŸाराधिकारी लेडीज सोसायटी फॉर नेटिव फीमेल एडुकेशन को नियुक्त किया जिसकी संरक्षिका लेडी एमहर्स्ट थी। डेविड हेयर इस संस्थान को वार्षिक चंदा दिया करते थे। गवर्नर जनरल लार्ड एमहर्स्ट की पत्नी लेडी एमहर्स्ट के प्रयासों से कलकता में बंगाल लेडीज सोसायटी का गठन हुआ। इस समिति ने 18 मई 1826 ई0 को आर्क डिकान कोरी के परामर्श से कलकता के कार्नवालिस एस्क्वायर के पूर्वी छोर पर सेंट्रल स्कूल की नींव डाली। लंदन मिशनरी सोसायटी कलकता से सम्बद्व विद्यालय जो उस समय कार्यरत थे उनमें छात्राओं की संख्या क्रमशः 45,25 और 28 थी। धीरे-धीरे लोग अपनी लड़कियों को इन स्कूलों में भेजने लगे। वर्द्वमान के स्कूलों में तो 14-15 वर्ष की नवयुवतियाँ भी पढ़ने जाया करती थी।
सिरामपुर मिशनरी के विलियम कैरी, मार्शमैन तथा वार्ड ने कुछ भारतीयों के सहयोग से 1823 ई0 में सिरामपुर और उसके आस-पास के क्षेत्रां में बालिका विद्यालयों की स्थापना का कार्य शुरु किया था। बंगाल के अतिरिक्त उन्होंने बनारस, इलाहाबाद तथा अराकान (बर्मा) में भी बालिकाओं के लिए स्कूल खोले। 1827 ई0 तक हुगली जिले में मिशनरियों द्वारा 12 कन्या पाठशालायें चलाई जाने लगी थी। एक वर्ष बाद लेडीज सोसायटी फॉर नेटीव फीमेल एडुकेशन इन कलकता एण्ड इट्स विसिनिटी ने एक विद्यालय मिस मेरी कुक के निर्देशन में स्थापित किया। ऐसा देखा गया कि गरीब इलाकों में खुले विद्यालयों के बारे में जानने के लिए मुस्लिम महिलायेंं भी दिलचस्पी ले रही थी। विलियम एडम्स के अनुसार इस समय सेन्ट्रल और क्रिश्चियन विलेज स्कूल स्त्री शिक्षा देने में संलग्न थे। सेन्ट्रल स्कूल में 138 और क्रिश्चियन विलेज स्कूलों में 14 बालिकाएँॅ शिक्षा ग्रहण कर रही थी।
कलकता के बाद मद्रास को ईसाई मिशनरियों ने महिला शिक्षा के विकास के केन्द्र के रूप में चुना। चर्च मिशन सोसायटी को दक्षिण भारत में अपेक्षाकृत अधिक सफलता मिली; दो सालों के अंदर नौ और पाठशालाएॅँ खोली गई। 1831 ई0 में इस सोसायटी ने अहमदाबाद में दो कन्या पाठशालाओं की स्थापना की । इसमें छात्रावास की भी व्यवस्था थी। विल्सन दम्पिŸा ने 1829 - 30 ई0 में बम्बई में छः बालिका विद्यालयों की स्थापना की थी; जिसमें 200 छात्रायें अध्ययन करती थी। चर्च मिशन सोसायटी ने मुम्बई प्रेसीडेंसी में पहली बार 1826 ई0 में बालिका विद्यालयों को स्थापित करना शुरु किया था और अगले 10 वर्षों के अंदर थाणे, बसिन तथा नासिक में लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना सोसायटी के द्वारा की गई। 1850 का साल समाप्त होते-होते मिशनरियों के प्रयास से नारी शिक्षा के 354 दिन में चलने वाले स्कूल खुल गए, जिनमें 1500 लडकियॉँ शिक्षा ग्रहण करती थी और उनमें से 91 आवासीय विद्यालय थे। देहरादून, सियालकोट और गुजरानवाला में प्रोवेस्ट्रियन चर्च ने छात्राओं के लिए कई स्कूल स्थापित किए थे।
महिला विद्यालयों में सबसे महत्वपूर्ण 1849 ई0 में जेम्स इल्वर्ट ड्रिंकवाटर बेथ्यून द्वारा हिन्दू कन्या विद्यालय की स्थापना कार्नवालिस एस्क्वायर कलकता में देशी भद्रपुरुषों की लड़कियों को शिक्षित करने के लिए किया गया था। बेथ्यून ने अपनी परियोजना में कुलीन परिवारों को सहभागी बनाने के लिए काफी प्रयत्न किया तथा ईश्वरचन्द्र विद्यासागर को सचिव नियुक्त किया। फलतः इस विद्यालय में पढ़नेवाली छात्राओं की संख्या 30 तक पहॅुँच गई। बेथ्यून ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी सारी चल - अचल सम्पिŸा इस विद्यालय के नाम कर दी थी। 1863 ई0 में इस विद्यालय में कुल 95 लड़कियाँं नामांकित थी जिनकी आयु 5 से 7 वर्ष के बीच थी तथा तीन-चौथाई छात्रायें निम्न जाति या गरीब परिवार से सम्बन्धित थी।
गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी (1848 - 1856) महिला शिक्षा को लाभदायक और महत्वपूर्ण मानता था। ‘शिक्षा का मैग्नाकार्टा‘ कही जानेवाली 1854 के वुड्स डिस्पैच में पुरुषों एवं महिलाओं को समान रुप से शिक्षा दिए जाने की बात कही गई थी।36 ब्रह्यसमाज के बंगाली सदस्यों ने महिला शिक्षा के प्रति होनेवाले सुधारों का प्रतिनिधित्व किया तथा राममोहन राय ने विधायिका सभा से अपील की कि कलकता के प्रत्येक मुहल्ले में लड़कियों के लिए विद्यालय स्थापित किये जाए। उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफी धन व्यय किए। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयत्नों से बालिकाओं के शिक्षण संस्थानों में उल्लेखनीय वृद्वि हुई। नवम्बर 1851 से 1858 तक उनके प्रयासों से लगभग 35 शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई थी। इन विद्यालयों में निः शुल्क शिक्षा दी जाती थी तथा प्रोत्साहनस्वरूप विद्यालय की तरफ से लेखन-सामग्री और पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती थी। उन्होंने महिला शिक्षा के प्रति जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से एक लेख प्रतियोगिता का आयोजन भी किया था जिसका शीर्षक था ’महिला शिक्षा की उपयोगिता’।37
यंग बंगाल आन्दोलन महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दां पर कुछ ज्यादा ही सक्रिय था। हिन्दू कॉलेज के स्नातक और प्रमुख समाजसुधारक पियारीचरण सरकार ने कलकता के बारासात मुहल्ले में स्थापित गवर्नमेंट स्कूल के प्रधानाध्यापक का पद संभाला। इस पद पर रहते हुए उन्होंने वारासात में कन्याओं के लिए एक निः शुल्क विद्यालय की स्थापना 1847 ई0 में की थी। बाद में इस विद्यालय का नाम कालीकृष्ण गर्ल्स हाई स्कूल पड़ा। शिक्षा सचिव के पद पर रहते हुए जे0 ई0 डी0 बेथ्यून ने इस विद्यालय का निरीक्षण किया था। इस समय इस विद्यालय को दक्षिणारंजन मुखर्जी, राजगोपाल घोष, मनमोहन तर्कांलंकार एवं ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का सक्रिय सहयोग मिल रहा था।
उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक महिला शिक्षा के विरोध में बंगाली समाज खड़ा था। समाचार दर्पण के सम्पादक ने 1831 में नारी शिक्षा के समर्थकों की आलोचना की थी, उसी वर्ष बंगदूत ने अपने 20 अगस्तवाले अंक में नारी शिक्षा का समर्थन किया था। कृष्णमोहन बनर्जी ने 1840 ई0 में इंडियन फीमेल एडुकेशन शीर्षक निबंध में लड़कियों को सार्वजनिक विद्यालयों में भेजने की अपेक्षा प्राइवेट ट्यूशनों को अच्छा बताया। बाबू प्रसन्न कुमार टैगोर ने यूरोप के ट्यूटरों को अपनी पुत्रियों को पढ़ाने के लिए रखा था। 24 दिसम्बर 1847 को कलकता में आयोजित एक नागरिक सभा में उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित हिन्दू लड़कियों को ईसाई विद्यालयों में पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। ब्रह्मसमाजी ईश्वरचद्र विद्यासागर ने स्कूल निरीक्षक के पद पर रहते हुए महिला शिक्षा का काफी प्रसार किया। 1849 ई0 में बेथ्यून के कन्या विद्यालय के सचिव पद पर रहते हुए उन्होंने भद्रलोक की महिलाओं को विद्यालय तक लाने में काफी जोर लगाया। अपने सरकारी हैसियत का फायदा उठाते हुए विद्यासागर ने नवम्बर 1847 से 1855 के बीच 40 गाँवों में लड़कियों के लिए विद्यालयों की स्थापना करवाई थी। 1858 में सरकार द्वारा छोटे सरकारी विद्यालयों को अनुदान बंद करने के नये नियम के विरोध में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया।
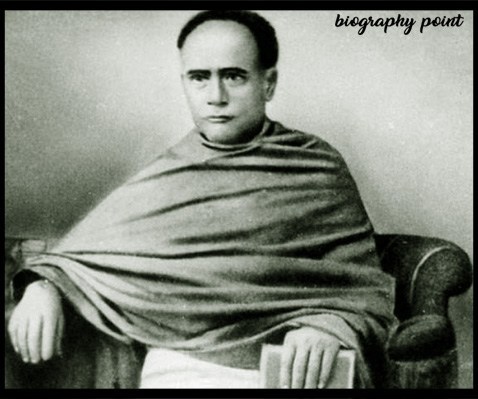
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें